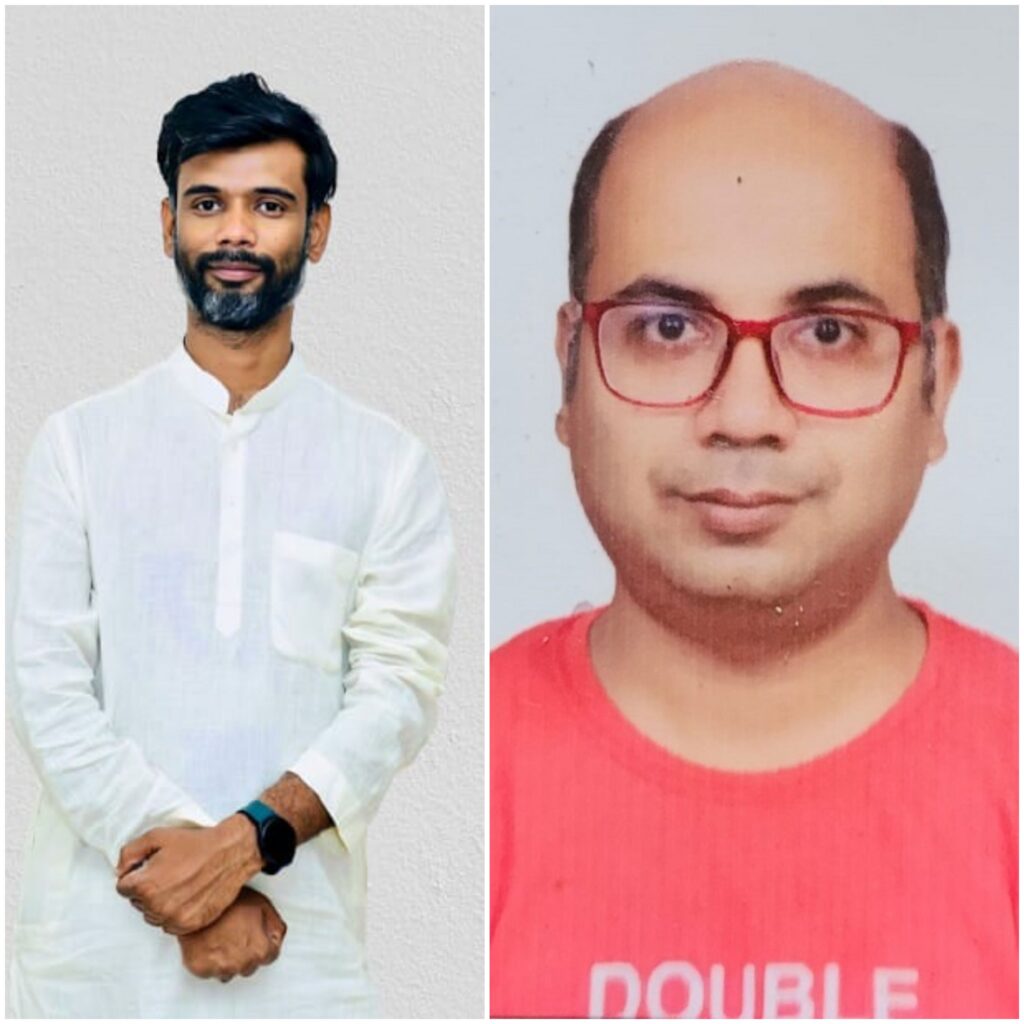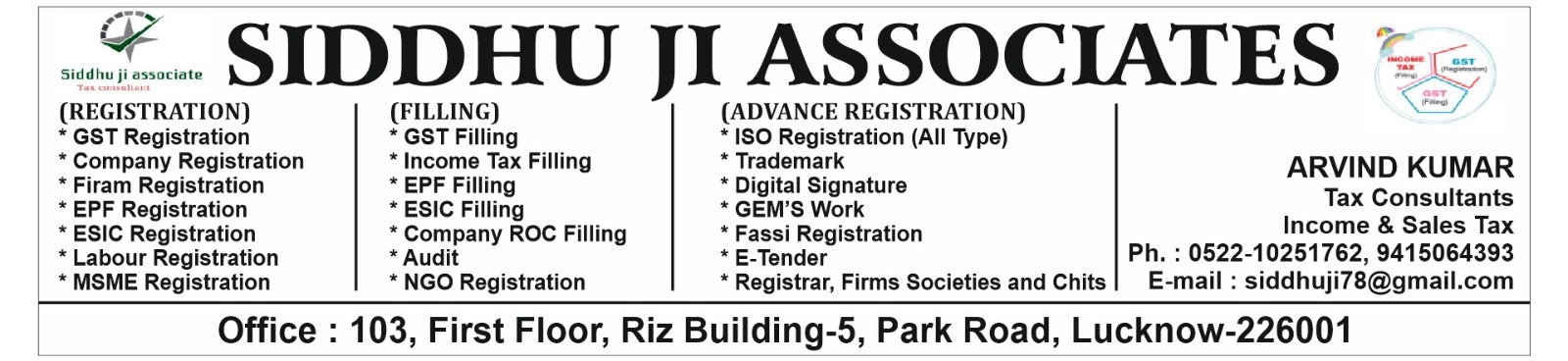आत्महत्या नहीं, सामाजिक-आर्थिक संकट की आवाज़ है – कब जागेगा भारत?
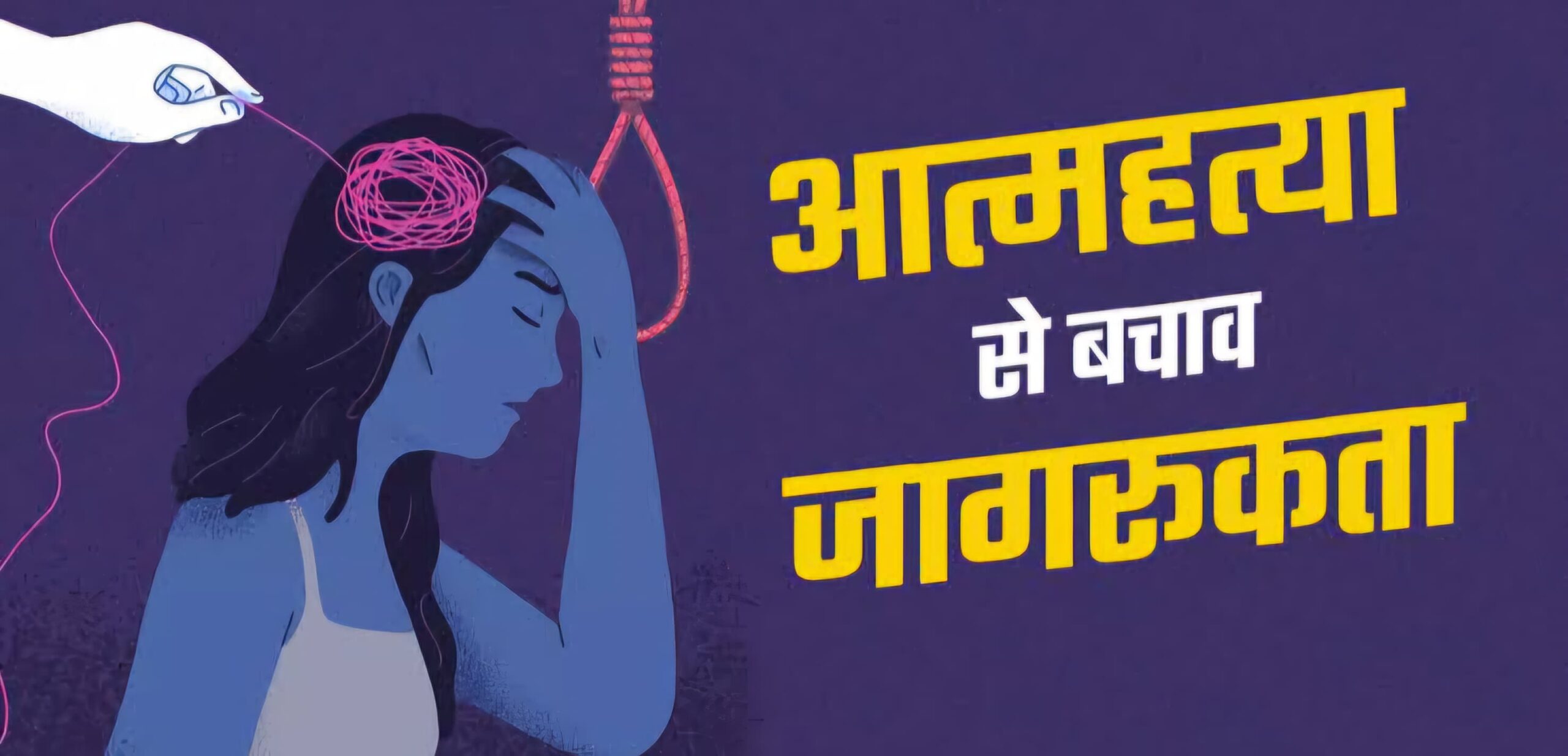
जिस तरह से समाज में युवाओं के मध्य आत्महत्या की दर बढ़ रही है, ये केवल एक सामाजिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय समस्या है ये एक प्रकार से आधुनिक सभ्यता की उपब्लिधयों की विषाक्त देन भी है अनियंत्रित उपभोग , सामाजिक संबधों में समसरता की कमी , काम की अनिमियतिता और बहुत कुछ पाने की चाहत मानसिक व्याधियों को जन्म देती हैं।
कई बार तो ये मानसिक व्याधियां महामारी का रूप धारण कर लेती हैं मानसिक तनाव एक ऐसी महामारी है जिसका निदान मनुष्यता को बचाये रखने के लिए आवयश्क है भारत में आत्महत्या अब केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रह गई है, बल्कि यह एक मानवीय और सामाजिक संकट का रूप ले चुकी है।
लान्सेट जर्नल की हालिया रिपोर्ट की रिपोर्ट कहती है कि आत्महत्या मानसिक स्वास्थ्य से कहीं ज्यादा सामाजिक—आर्थिक कारकों का परिणाम है, जिनमें गरीबी, कर्ज, घरेलू हिंसा, व्यसन और अलगाव जैसे तत्व शामिल हैं यह बदलाव मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित नैरेटिव से हटकर एक व्यापक सार्वजनिक-स्वास्थ्य दृष्टिकोण अपनाने की वकालत करता है। सरकारी आंकड़ों में यह स्पष्ट झलकता है: 2022 में NCRB ने भारत में आत्महत्या की संख्या 1.71 लाख दर्ज की, जो प्रति 1,00,000 लोगों पर 12.4 की सर्वाधिक दर थी—इसमें 18–45 वर्ष के युवा 67 प्रतिशत मामलों में शामिल हैं । यह विकराल स्थिति संदेश देती है कि आत्महत्या केवल मानसिक कमजोरी का परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक और संरचनात्मक टूट का प्रतीक है। गरीबी, अव्यवस्थित उपभोग, बेरोज़गारी, कर्ज का दबाव, संबंधों में टूट और घरेलू असुरक्षाये सभी कारण लान्सेट शोध में आत्महत्या की प्रमुख वजहों के रूप में प्रमाणित हैं ।
विशेषकर बेरोज़गार महिलाओं में आत्महत्या की दर 94.8 प्रति 1,00,000 है, जो नौकरीपेशा महिलाओं (12.6 प्रति 1,00,000) से कहीं अधिक है आज मानसिक तनाव एक महामारी की शक्ल में उभर रहा है, जिसमें अकेलापन, रिश्तों का टूटना और उपभोगवादी जीवनशैली मिलकर युवा पीढ़ी को आत्मघाती प्रवृत्ति की ओर ले जा रहे हैं। AIIMS के प्रोफेसर बताते हैं कि भारत में युवा वर्ग में आत्महत्या वैश्विक औसत की तुलना में लगभग दोगुनी है, और हर दिन 160 युवा इस कगार पर पहुँचते हैं । सरकार की 2022 वाली National Suicide Prevention Strategy में मानसिक स्वस्थ्य पर बल दिया गया, लेकिन लान्सेट रिपोर्ट बताती है कि अब सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण शामिल करना अनिवार्य है| गरीबी निवारण, कर्ज राहत, घरेलू हिंसा रोधी योजनाएँ और बेरोज़गारी से निपटने वाले कदम जैसे इन मूलभूत उपायों से ही युवाओं का मानसिक व्याधिपन दूर किया जा सकता है | एक प्रभावी रणनीति के लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ही नहीं, बल्कि वित्त, शिक्षा, महिला-कल्याण, श्रम, और सामाजिक न्याय मंत्रालयों को भी शामिल किया जाए। मीडिया में रिपोर्टिंग को जिम्मेदार और संवेदनशील बनाना, तथा स्कूल और कॉलेजों में “गेटकीपर ट्रेनिंग” और सहज इमोशनल सपोर्ट नेटवर्क सक्रिय करना किसी उपाय से कम नहीं है ।
भारत, जहाँ विश्व की आबादी का 18 प्रतिशत हिस्सा रहता है, एक महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है, मानसिक विकार विकलांगता के साथ जीने वाले वर्षों (वाईएलडी) का दूसरा प्रमुख कारण है और कई राज्यों में आत्महत्या मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है।
राष्ट्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि भारत की 15 प्रतिशत वयस्क आबादी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है, जो इन समस्याओं से निपटने के लिए हस्तक्षेप की मांग करती है, फिर भी उपचार में काफी गैप रह जाता है और यह गैप 70-92 प्रतिशत तक है, जिससे लाखों लोग देखभाल के बिना रह जाते हैं।
हालाँकि 2017 का मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य तक पहुँच को एक सांविधिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है, फिर भी भारत में 11 करोड़ से अधिक लोग अभी भी मानसिक स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत मदद नहीं मांगते हैं। हर वर्ष एक लाख से अधिक लोग आत्महत्या करके मर जाते हैं, जबकि अनगिनत अन्य लोग अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश करते हैं और यह स्थिति हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।
इस अंतर को पाटने और मानसिक स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए टेली एमएएनएएस की स्थापना की गई थी। टेलीफोन के माध्यम से परामर्श, मनोचिकित्सा और रेफरल सेवाएं प्रदान करके, यह कार्यक्रम उन लोगों को एक एक जीवन रेखा मुहैया कराती है जो अन्यथा मदद लेने में असमर्थ हो सकते हैं। ज्यादातर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसको प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि मानसिक बीमारी के कारण किसी भी व्यक्ति को भेदभाव या उपेक्षा का सामना न करना पड़े।
ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में भी आत्महत्या की समस्या बड़ी विकराल है और दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में लगभग 150 आई आई टी के छात्रों ने अपनी जीवन लीला का अंत किया | क्या ये हमारी सभ्यता की प्रगति के मुंह पर तमाचा नहीं है | क्या हम एक ‘मानसिक रूप से असफल’ समाज हैं? ज़रूरत है सिर्फ आत्मनिरीक्षण की—जब कर्ज, बेरोज़गारी और टूटे रिश्ते युवा पीढ़ी को आत्महत्या की ओर धकेलते हैं, तो यह हमारी नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उन्हें अकेले न छोड़ें। हमें एक मानवतावादी, सहानुभूतिपूर्ण और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनने का मार्ग चुनना होगा, ताकि युवा फिर से विश्वास के साथ भविष्य की ओर बढ़ सकें।
जो राष्ट्र अपने नागरिकों को एक स्वस्थ मानसिक समाज देने में विफल होता है वो प्रगति के केवल झठे आंकड़े प्रस्तुत करता है उन्नति का ये पैमाना ही नीति निर्माताओं को नई दृष्टि देगा और हम अपने लोगों को इस विकराल दानव से बचा पायेगें क्योंकि ये दानव रक्तबीज की तरह बढ़ता ही जा रहा है।