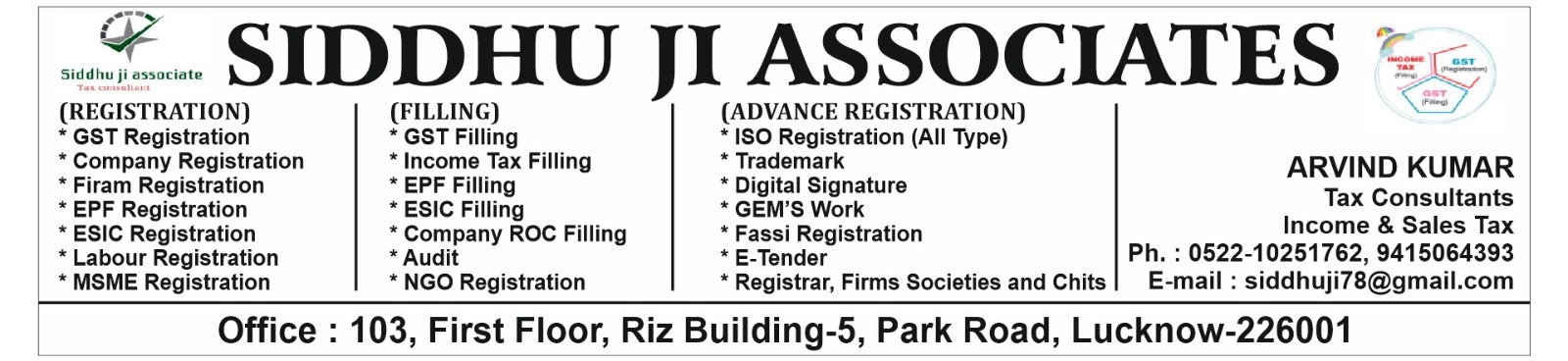अंतरराष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस पर विशेष : सांस्कृतिक बौद्धिकता का आधार मातृ भाषा में चिंतन है !
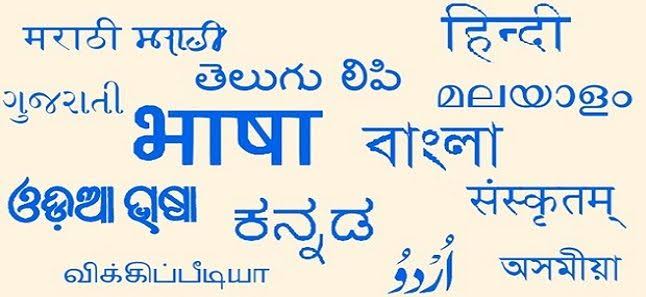
जब शिशु माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो जिस भाषा में वह स्नेह, वात्सल्य, भावनाओं और प्रेम का आभास करता है, वही उसकी मातृ भाषा बनती है। यह भाषा केवल शब्दों का संचार नहीं होती, बल्कि यह उस शिशु की भावनाओं, संस्कारों, और उसकी सांस्कृतिक पहचान का संवेदनशील प्रतिबिम्ब है| मातृ भाषा में न केवल एक गहरी भावना समाहित होती है, बल्कि यह सांस्कृतिक बौद्धिकता का आधार भी है। यही वह भाषा है, जिसमें नवाचार और उच्च विचार की संभावनाएँ और संभावनाओं का विकास होता है।
मातृ भाषा में प्रेम की बृहत् भावनाएं और ज्ञान का भंडार निहित होता है | यही वह भाषा है जो हमारे अंतर्दृष्टि और चिंतन की शुद्धता को बनाये रखती है। लेकिन विकास की प्रक्रिया में जब बोलियों और भाषाओं का विनाश होता है, तो इसका अर्थशास्त्र भी संकट में पड़ता है। अंग्रेजी का एकाधिकार हमारी भाषाओं के चिंतन और सृजन को कमजोर कर देता है। आज हमें यह समझना होगा कि मातृ भाषा केवल संप्रेषण का साधन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना का ऊर्जा-प्रद स्रोत है। यह मनुष्य के जीवन काल तक उसे सीखने और समझने की प्रेरणा देती है।
भारत जैसी भाषायी विविधता से भरपूर भूमि में मातृ भाषा की महत्ता और भी बढ़ जाती है। मातृ भाषा में चिंतन और सृजन की एक अपूर्व क्षमता छिपी हुई है। यही वह भाषा है, जिसमें बौद्धिकता के प्रतिमान को प्राप्त किया जा सकता है। इसके द्वारा किसी भी समाज के संज्ञानात्मक और रचनात्मक अभिरुचि का विस्तार संभव है। यदि हमें अपने समाज में वास्तविक बौद्धिकता और विकास की ओर बढ़ना है, तो मातृ भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाना आवश्यक है।
यह केवल प्राथमिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर भी मातृ भाषा का प्रसार होना चाहिए। इससे न केवल ज्ञान की नवीनता बढ़ेगी, बल्कि विभिन्न विषयों के अनुवाद और शोध की दक्षता भी प्राप्त होगी। हालांकि, सैद्धांतिक रूप से यह विचार आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन इसका व्यावहारिक रूप में सफलता प्राप्त करना एक बड़ा प्रश्न है।
यह सवाल भाषा के अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी शिक्षा नीति पर निर्भर करती है। पूर्ववर्ती शिक्षा नीतियों और योजनाओं में भाषा के अर्थशास्त्र की ओर कम ध्यान दिया गया है, लेकिन अब समय आ गया है कि इस पर विचार किया जाए। भाषा का अपना एक अर्थशास्त्र होता है, जो आर्थिक असमानताओं से भी जुड़ा है। दुनिया की कई बोलियाँ और भाषाएँ विलुप्त होने के कगार पर हैं, और यह स्थिति केवल अर्थशास्त्र से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विकास से भी जुड़ी हुई है।
हमारे राष्ट्र के विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी मातृ भाषाओं का संरक्षण करें। जिस विकास मॉडल में हमारी सांस्कृतिक धरोहर और भाषाएँ लुप्त होती हैं, वह केवल विनाश की ओर अग्रसर करता है। भाषाओं का विलुप्त होना किसी राष्ट्र के सांस्कृतिक आत्मा के मरने जैसा है। अगर हम इस नुकसान को रोकने में विफल रहते हैं, तो हमारा विकास केवल एक मिथक बनकर रह जाएगा।
भारत में भाषाओं का विलुप्त होना एक गंभीर चिंता का विषय है। 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 भाषाएँ थीं, जो 1971 में घटकर 808 रह गईं। 2013 तक यह संख्या केवल 780 रह गई, और पिछले 50 वर्षों में 220 भाषाएँ विलुप्त हो चुकी हैं। यह केवल भारत की ही नहीं, बल्कि वैश्विक चिंता का विषय है।
वैज्ञानिक शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि जिन छात्रों ने अपनी मातृ भाषा में अध्ययन किया, उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्रों से कहीं बेहतर अनुसंधान कार्य किए। उदाहरण के लिए, भारतीय वैज्ञानिक सी. वी. श्रीनाथ ने अपने शोध में यह बताया था कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से अभियांत्रिकी की पढ़ाई करने वाले छात्र उच्च गुणवत्ता में अनुसंधान करते हैं। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि मातृ भाषा में चिंतन और सृजन के लिए एक विशेष प्रकार की मानसिकता और दक्षता विकसित होती है।
आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए मातृ भाषा का संरक्षण और संवर्धन आवश्यक है। यह केवल भाषाओं का बचाव नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का भी एक अहम पहलू है। लोहिया ने सही कहा था कि अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई से न केवल अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में कमी आती है, बल्कि यह शिक्षा और शोध की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है।
नई शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषावाद का मुद्दा उठाया गया है, लेकिन यह केवल सतही रूप में ज्ञान के केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। यदि हम बहुभाषावाद को आर्थिक प्रगति और भाषा के अर्थशास्त्र से जोड़ना चाहते हैं, तो गांधी, विनोबा और लोहिया के भाषा विमर्श को समझना अत्यंत आवश्यक है। हमें अपने ज्ञान के विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देना होगा, तभी हम एक सशक्त और समावेशी समाज का निर्माण कर सकेंगे।
अंत में, यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि हम मातृ भाषा में चिंतन और सृजन की प्रक्रिया को महत्व देते हैं, तो हम न केवल अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचा पाएंगे, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक सशक्त और समृद्ध समाज की ओर भी अग्रसर होंगे। मातृ भाषा का संरक्षण ही हमें बौद्धिक और सांस्कृतिक बौद्धिकता के असली सार तक पहुंचने में मदद करेगा।